Class 12 Hindi Aaroh Shamsher Bahadur Singh Usha
शमशेर बहादुर सिंह: उषा
Class 12 Hindi Aaroh Shamsher Bahadur Singh Usha : ‘उषा’ शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित एक अत्यंत सुंदर और बिंबधर्मी कविता है। यह कविता सूर्योदय से ठीक पहले के क्षणों में प्रकृति में होने वाले पल-पल के परिवर्तन का एक अद्भुत शब्द-चित्र प्रस्तुत करती है। कवि भोर के समय बदलते हुए आकाश को गाँव के घरेलू जीवन से जुड़े सरल और सहज उपमानों के माध्यम से चित्रित करता है।
कवि दिखाता है कि कैसे भोर का आसमान कभी नीले शंख जैसा लगता है, तो कभी राख से लीपे हुए गीले चौके जैसा। कभी वह लाल केसर से धुल गई काली सिल प्रतीत होता है, तो कभी स्लेट पर लाल खड़िया चाक मलने जैसा। इन उपमाओं के माध्यम से कवि प्रकृति की सुंदरता को मानवीय जीवन की संवेदनाओं से जोड़ता है। कविता का अंत तब होता है जब सूर्योदय होने लगता है और उषा का जादू टूट जाता है, जो यह दर्शाता है कि हर सुंदरता क्षणभंगुर है, लेकिन उसका प्रभाव स्थायी होता है।
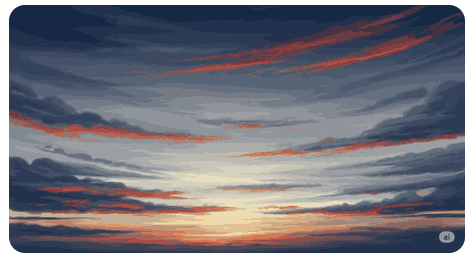
कवि परिचय
जन्म: शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी, 1911 को देहरादून (अब उत्तराखंड में) हुआ था।
प्रकाशित रचनाएँ: ‘कुछ कविताएँ’, ‘कुछ और कविताएँ’, ‘चुका भी हूँ नहीं मैं’, ‘इतने पास अपने’, ‘बात बोलेगी’, ‘काल तुझसे होड़ है मेरी’ आदि। उन्होंने ‘उर्दू-हिंदी कोश’ का संपादन भी किया।
सम्मान: उन्हें ‘साहित्य अकादेमी’ और ‘कबीर सम्मान’ सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
निधन: सन् 1993 में अहमदाबाद में उनका निधन हो गया।
काव्यगत विशेषताएँ
शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी और उर्दू का ‘दोआब’ माना जाता है। उनकी कविताएँ साहित्य, चित्रकला और संगीत का एक अद्भुत संगम हैं। वे बिंबधर्मी कवि के रूप में जाने जाते हैं, जो शब्दों के माध्यम से जीवंत चित्र बनाते हैं। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को मिटा देता है और भाषा से परे जाकर अपनी बात कहना चाहता है।
वे विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि हैं। उनकी भाषा पर उर्दू शायरी का गहरा प्रभाव है, जिसमें संज्ञा और विशेषण के बजाय सर्वनामों, क्रियाओं और मुहावरों का अधिक प्रयोग मिलता है। उनकी कविता केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि सुनने और देखने के लिए भी पाठक को प्रेरित करती है।
कविता ‘उषा’ का सार
‘उषा’ कविता सूर्योदय से ठीक पहले के पल-पल बदलते प्राकृतिक दृश्यों का एक अद्भुत शब्द-चित्र है। इस कविता में कवि ने भोर के आसमान की सुंदरता को गाँव के सुबह के जीवन से जोड़ा है।
कविता में, भोर के नीले आकाश की तुलना नीले शंख से की गई है, फिर उसे राख से लीपे हुए चौके (रसोई) की तरह बताया गया है जो अभी भी गीला है। इसके बाद, कवि ने आसमान को काली सिल की तरह देखा, जिस पर लाल केसर लगा हो, या स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी गई हो। ये सभी उपमान गाँव के घरेलू जीवन से लिए गए हैं, जो कविता को एक सहज और मानवीय स्पर्श देते हैं।
कविता का अंत तब होता है जब सूर्योदय हो जाता है और उषा का जादू टूट जाता है। यह कविता प्रकृति की गति और सुंदरता को दर्शाती है, साथ ही यह संदेश भी देती है कि हर अंधकार के बाद उजाला आता है।
कविता – उषा
प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे।
भोर का नभ
राख से लीपा हुआ चौका
(अभी गीला पड़ा है)
बहुत काली सिल ज़रा से लाल केसर से
कि जैसे धुल गई हो
स्लेट पर या लाल खड़िया चाक
मल दी हो किसी ने
नील जल में या किसी की
गौर झिलमिल देह
जैसे हिल रही हो।
जादू टूटता है इस उषा का अब
सूर्योदय हो रहा है।
कविता के साथ
1. कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गाँव की सुबह का गतिशील शब्दचित्र है?
‘उषा’ कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने ऐसे अनेक उपमानों का प्रयोग किया है जो स्पष्ट रूप से गाँव की सुबह और उसकी गतिविधियों का गतिशील शब्दचित्र प्रस्तुत करते हैं:
- ‘राख से लीपा हुआ चौका‘: यह सबसे प्रमुख उपमान है जो सीधे गाँव के ग्रामीण परिवेश से जुड़ा है। गाँव में आज भी सुबह-सुबह घर के आँगन या रसोईघर (चौका) को राख से लीपकर स्वच्छ किया जाता है। यह एक ऐसी क्रिया है जो सुबह की ताज़गी और स्वच्छता का आभास देती है और ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग है। ‘अभी गीला पड़ा है’ विशेषण इस क्रिया के हाल ही में होने और सुबह की ताज़गी को दर्शाता है।
- ‘बहुत काली सिल ज़रा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो‘: ‘सिल’ गाँव के घरों में मसाला पीसने के लिए प्रयोग होने वाला एक पत्थर का उपकरण है। इस पर लाल केसर (लाल मिर्च या हल्दी) के अवशेष का दिखना और फिर उसका धुल जाना, यह दर्शाता है कि सुबह-सुबह भोजन बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह भी ग्रामीण रसोईघर और सुबह की दैनिक क्रियाओं का बिंब है।
- ‘स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने‘: यह उपमान भी गाँव के बच्चों और उनके स्कूल जाने या खेलने से जुड़ा है। गाँव के बच्चे अक्सर स्लेट पर खड़िया या चाक से लिखते-पढ़ते हैं। सुबह के आसमान के रंग को स्लेट और उस पर चाक मलने से जोड़ना, ग्रामीण शिक्षा और बच्चों की मासूमियत को दर्शाता है।
ये सभी उपमान सीधे-सीधे ग्रामीण जीवन, उसके औजारों, दैनिक क्रियाकलापों और वातावरण से संबंधित हैं। कवि ने इन्हीं के माध्यम से उषा के पल-पल बदलते रूप को जीवंत और गतिशील बनाया है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह किसी शहरी सुबह का नहीं, बल्कि एक गाँव की सुबह का यथार्थवादी और सौंदर्यपूर्ण चित्रण है।
2. भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका (अभी गीला पड़ा है) नयी कविता में कोष्ठक, विराम चिह्नों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है? समझाइए।
नयी कविता में, विशेषकर शमशेर जैसे बिंबधर्मी कवियों की कविताओं में, कोष्ठक, विराम चिह्नों और पंक्तियों के बीच का स्थान (whitespace) केवल व्याकरणिक या संरचनात्मक नहीं, बल्कि अर्थगत महत्व रखता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्ठक ‘(अभी गीला पड़ा है)‘ के प्रयोग से कविता में निम्नलिखित विशेष अर्थ पैदा हुए हैं:
- गतिशीलता और ताजगी का बोध: ‘राख से लीपा हुआ चौका’ अपने आप में एक स्थिर बिंब है, लेकिन कोष्ठक में दिया गया ‘अभी गीला पड़ा है’ उसे एक गतिशील, जीवंत और तात्कालिकता का एहसास देता है। यह बताता है कि चौके को अभी-अभी लीपा गया है, यानी सुबह की ताज़गी और साफ-सफाई की क्रिया हाल ही में संपन्न हुई है। यह क्रियाशील बिंब उषा के बदलते रंग और समय के बीतने की गति को दर्शाता है।
- सजीव चित्रण और यथार्थवाद: कोष्ठक का प्रयोग पाठक को उस दृश्य के बिल्कुल करीब ले जाता है। यह एक टिप्पणी या फुटनोट की तरह है जो दृश्य की वास्तविकता को और पुष्ट करता है। यह बिंब को केवल देखने योग्य नहीं, बल्कि अनुभव करने योग्य बनाता है – पाठक को उस गीलेपन का, उस ताजगी का एहसास कराता है।
- क्षणभंगुरता का संकेत: ‘अभी गीला पड़ा है’ यह भी दर्शाता है कि यह स्थिति क्षणभंगुर है। जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, चौका सूख जाएगा। यह उषा के पल-पल बदलते सौंदर्य की अस्थिरता और अस्थायी प्रकृति को रेखांकित करता है। कवि यह बताना चाहता है कि यह सुंदरता एक क्षणिक अनुभव है जिसे तत्काल महसूस किया जाना चाहिए।
- चित्रात्मकता में गहराई: कोष्ठक का प्रयोग चित्र को और अधिक ‘सजीव’ बनाता है। यह पाठक के मन में एक अतिरिक्त विवरण जोड़ता है जो उस दृश्य को अधिक पूर्ण और विश्वसनीय बनाता है। यह एक चित्रकार के ब्रुशस्ट्रोक की तरह है जो एक छोटे से विवरण से पूरे चित्र को जीवंत कर देता है।
- सहज बातचीत की शैली: कोष्ठक का प्रयोग कई बार कवि की चिंतन प्रक्रिया या पाठक से सीधे संवाद के रूप में भी देखा जा सकता है, जैसे वह बात करते-करते कोई अतिरिक्त, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हो। यह कविता में एक सहज, अनौपचारिक और बोलचाल का लहजा लाता है।
इस प्रकार, कोष्ठक का यह प्रयोग ‘उषा’ कविता को केवल एक दृश्य चित्र नहीं, बल्कि एक गतिशील, सजीव और अनुभूतियों से भरा शब्द-चित्र बनाता है, जिसमें समय और स्थान की विशिष्टता स्पष्ट होती है।
कविता के आसपास
1. अपनी रचना: अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्दचित्र खींचिए।
(क) सूर्योदय का शब्दचित्र:
भोर का नभ, जैसे किसी गाँव की धुली हुई कढ़ाई में धीरे-धीरे पिघल रहा हो सोना। पूरब की खिड़की से झाँकता सूरज का पहला कतरा, खेतों की मेढ़ों पर पसरी ओस को चुम्बन से सुखाता। घरों के धुएँ से उठता हुआ आलस्य और चाय की महक, पगडंडियों पर चलने लगे हैं साइकिल की घंटी और मंदिर की घंटियों की आवाज़, जैसे जीवन की नई धुन शुरू हो रही हो।
(ख) सूर्यास्त का शब्दचित्र:
दिन का काम समेटता सूरज, जैसे थककर लाल होता लोहार का हथौड़ा। आसमान में बिखरती सिंदूरी रंगत, मौन साध चुकी हो जैसे किसी पुरानी हवेली की छत। दूर किसी मस्जिद से आती अजान, और पेड़ों से लौटते पंछियों का शोर, घर लौटते जानवरों के खुरों की थाप। मिट्टी के चूल्हों से उठता धुआँ, रोशनी में ढलती परछाइयाँ लंबी होतीं, जैसे दिन अपने पैरों पर खड़ा होकर अंधेरे में समा रहा हो। एक गहरी शांति फैलती है, और रात की चादर धीरे से धरती को ओढ़ लेती है।
2. सूर्योदय का वर्णन लगभग सभी बड़े कवियों ने किया है। प्रसाद की कविता “बीती विभावरी जाग री‘ और अज्ञेय की “बॉवरा अहेरी‘ की पंक्तियाँ आगे बॉक्स में दी जा रही हैं। ‘उषा‘ कविता के समानांतर इन कविताओं को पढ़ते हुए नीचे दिए गए बिंदुओं पर तीनों कविताओं का विश्लेषण कीजिए और यह भी बताइए कि कौन-सी कविता आपको ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों?
- प्रसाद की कविता: “बीती विभावरी जाग री!” अंबर पनघट में डुबो रही- तारा-घट ऊषा नागरी। खग-कुल कुल-कुल-सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई- मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए– तू अब तक सोई है आली आँखों में भरे विहाग री।
- अज्ञेय की कविता: “बावरा अहेरी” (पंक्तियाँ नहीं दी गई हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा) (सामान्य रूप से, अज्ञेय की ‘बावरा अहेरी’ में सूर्योदय को एक शिकारी (अहेरी) के रूप में चित्रित किया गया है जो अपनी सुनहरी किरणों के जाल से अंधकार का शिकार करता है।)
- शमशेर बहादुर सिंह की कविता: “उषा” प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका (अभी गीला पड़ा है) बहुत काली सिल ज़रा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है।
तीनों कविताओं का विश्लेषण:
क) उपमान:
- जयशंकर प्रसाद (‘बीती विभावरी जाग री!‘): प्रसाद की कविता में सूर्योदय के लिए मुख्य उपमान मानवीकरण और संस्कृतनिष्ठ बिंब हैं। उषा को एक चतुर ‘नागरी’ (नायिका) के रूप में चित्रित किया गया है जो आकाश रूपी पनघट में तारों (घट) को डुबो रही है। लता को भी मुकुलों से रस भरते हुए दिखाया गया है। ये उपमान कोमल, लाक्षणिक और सौंदर्यवादी हैं, जो प्रकृति को स्त्री रूप में प्रस्तुत करते हैं।
- शमशेर बहादुर सिंह (‘उषा‘): शमशेर की कविता में उपमान ग्रामीण परिवेश और दैनिक जीवन से लिए गए हैं। ‘नीला शंख’, ‘राख से लीपा हुआ चौका (अभी गीला पड़ा है)’, ‘बहुत काली सिल ज़रा से लाल केसर से धुल गई हो’, ‘स्लेट पर लाल खड़िया चाक मलना’, ‘नील जल में गौर झिलमिल देह का हिलना’ जैसे उपमान सीधे-सीधे घर-आँगन, रसोई और बच्चों के खेल से संबंधित हैं। ये उपमान दृश्य, स्पर्श और गति तीनों का अनुभव कराते हैं।
- अज्ञेय (‘बावरा अहेरी‘): अज्ञेय की कविता में सूर्योदय के लिए उपमान शिकारी (अहेरी) का है। सूर्य को एक शिकारी के रूप में देखा जाता है जो अपनी ‘सुनहली किरणों’ के बाणों से अँधेरे का शिकार करता है। यह उपमान अधिक प्रतीकात्मक, क्रियाशील और चिंतनपरक है, जो प्रकृति में एक पुरुषवादी शक्ति का प्रदर्शन करता है।
ख) शब्दचयन:
- जयशंकर प्रसाद: प्रसाद का शब्दचयन संस्कृतनिष्ठ, तत्सम प्रधान और कोमलकांत पदावली से युक्त है (‘विभावरी’, ‘अंबर पनघट’, ‘तारा-घट’, ‘खग-कुल’, ‘किसलय’, ‘मधु मुकुल’, ‘अमंद’, ‘मलयज’, ‘विहाग’)। उनकी भाषा में एक गेयता और मधुरता है, जो एक रोमांटिक और स्वप्निल वातावरण निर्मित करती है।
- शमशेर बहादुर सिंह: शमशेर का शब्दचयन सहज, घरेलू और बिंबात्मक है। उन्होंने सरल, बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है जो सीधे-सीधे दृश्य को उपस्थित करते हैं (‘शंख’, ‘राख’, ‘चौका’, ‘गीला’, ‘सिल’, ‘केसर’, ‘स्लेट’, ‘खड़िया’, ‘चाक’)। उनके शब्द चित्र-निर्माण पर अधिक केंद्रित हैं और उनमें एक प्रकार की चुप्पी और ठहराव के बीच गति का अहसास होता है।
- अज्ञेय: अज्ञेय का शब्दचयन अधिक प्रतीकात्मक, दार्शनिक और नवीन है। उनकी भाषा में एक बौद्धिकता और तीक्ष्णता होती है, जो अमूर्त भावों को व्यक्त करने में सक्षम होती है। ‘अहेरी’, ‘बावरा’, ‘सुनहले तीर’ जैसे शब्द उनके विशिष्ट शैली का हिस्सा हैं।
ग) परिवेश:
- जयशंकर प्रसाद: प्रसाद की कविता का परिवेश प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांटिक भावुकता से भरा है। यह एक अमूर्त, सार्वभौमिक सुबह का चित्रण है जहाँ प्रकृति को एक भावुक और संवेदनशील नायक/नायिका के रूप में देखा गया है। यह शहरी या ग्रामीण किसी विशेष परिवेश से बंधा नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक सौंदर्य लोक रचता है।
- शमशेर बहादुर सिंह: शमशेर की कविता का परिवेश विशिष्ट रूप से ग्रामीण और घरेलू है। ‘चौका’, ‘सिल’, ‘स्लेट’ जैसे उपमान इसे गाँव के सुबह के जीवन से जोड़ते हैं। यह एक यथार्थवादी चित्रण है जहाँ सुबह की प्रकृति का परिवर्तन ग्रामीण जीवन की गतिविधियों के साथ गुंथा हुआ है।
- अज्ञेय: अज्ञेय की कविता का परिवेश अधिक वैचारिक और प्रतीकात्मक है। यह प्रकृति को किसी विशेष भौगोलिक या सामाजिक संदर्भ में नहीं, बल्कि एक दार्शनिक या existentialist दृष्टिकोण से देखती है। यह सूर्योदय के पीछे की शक्ति, गति और उद्देश्य पर अधिक केंद्रित है।
कौन-सी कविता ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों?
यह व्यक्तिगत पसंद का विषय है। हालाँकि, मुझे शमशेर बहादुर सिंह की ‘उषा‘ कविता ज़्यादा अच्छी लगी और इसके कई कारण हैं:
- जीवंत बिंबात्मकता: ‘उषा’ कविता में दृश्य बिंबों की एक अद्भुत श्रृंखला है जो पल-पल बदलती सुबह को साकार कर देती है। ‘राख से लीपा हुआ चौका (अभी गीला पड़ा है)’, ‘काली सिल लाल केसर से धुल गई हो’, ‘स्लेट पर लाल खड़िया चाक मलना’, ‘नील जल में गौर झिलमिल देह का हिलना’ – ये सभी बिंब इतने सजीव और नवीन हैं कि वे पाठक को सीधे उस सुबह का अनुभव करा देते हैं।
- यथार्थवादी और घरेलू स्पर्श: कविता में गाँव के घरेलू जीवन के उपमानों का प्रयोग इसे बहुत relatable और यथार्थवादी बनाता है। यह हमें किसी काल्पनिक लोक में नहीं ले जाता, बल्कि हमारे अपने आसपास की सुबह से जोड़ता है।
- गतिशीलता और परिवर्तन: कवि ने सुबह के हर बदलते रंग और रूप को इतनी खूबसूरती से शब्दों में ढाला है कि कविता में एक निरंतर गति और प्रवाह का अनुभव होता है, जैसे हम स्वयं उस परिवर्तन के साक्षी बन रहे हों। ‘जादू टूटता है इस उषा का अब, सूर्योदय हो रहा है’ पंक्ति में अचानक आए परिवर्तन का अहसास बहुत प्रभावी है।
- संवेदी अनुभव: शमशेर की कविता केवल दृश्य ही नहीं, बल्कि स्पर्श (गीला चौका), रंग (नीला, लाल, काला), और गति (देह का हिलना) के माध्यम से एक पूर्ण संवेदी अनुभव प्रदान करती है।
जबकि प्रसाद की कविता अपनी गेयता और लाक्षणिकता में सुंदर है, और अज्ञेय की कविता अपनी बौद्धिकता और प्रतीकात्मकता में प्रभावशाली है, शमशेर की ‘उषा’ अपनी अद्वितीय बिंबात्मकता, ग्रामीण यथार्थ और गतिशील चित्रण के कारण मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है और एक ऐसी सुबह का चित्र उकेरती है जिसे हम अपनी आँखों के सामने घटित होते हुए महसूस कर सकते हैं।